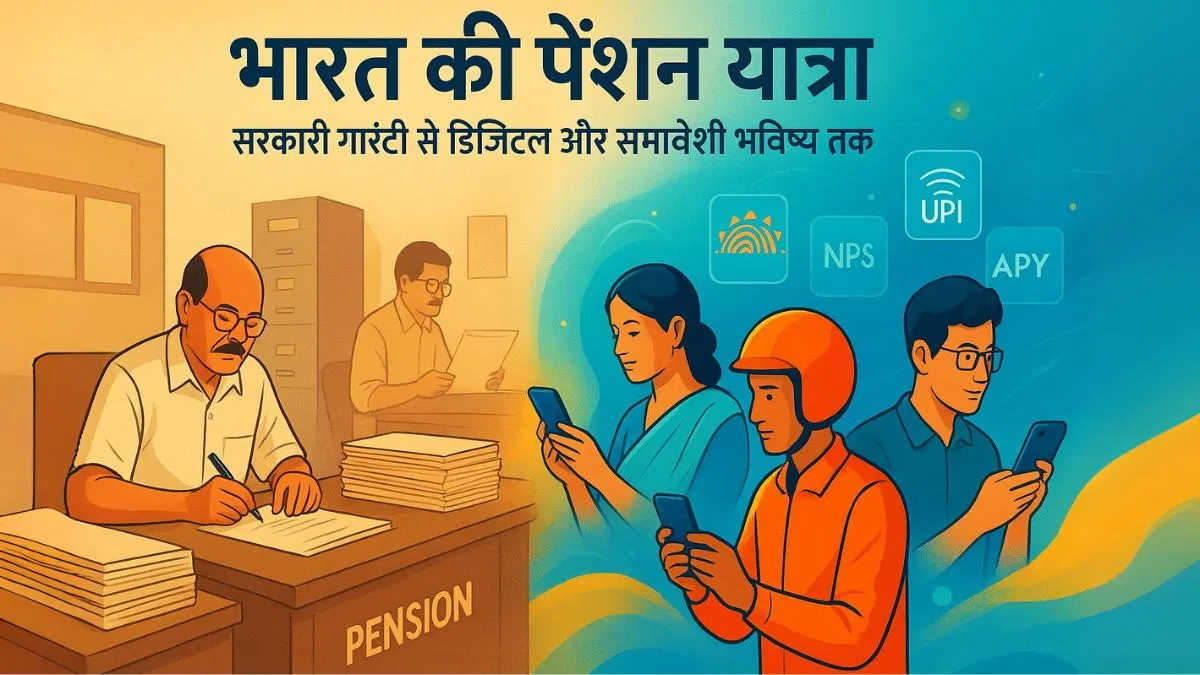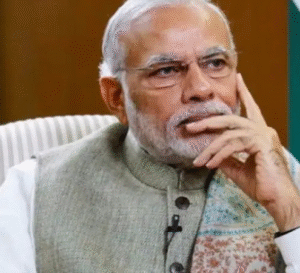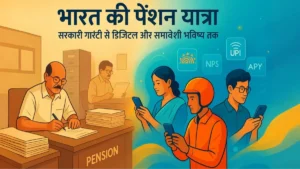भारत में 1970 और 1980 के दशक के दौरान सेवानिवृत्ति बेहद सरल सी अवधारणा थी जो सिर्फ एक ही तरह की थी. सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत लोगों के लिए, पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ ही नहीं, बल्कि एक आश्वासन था, देखभाल की निरंतरता का जो राज्य की संरक्षक और प्रदाता के रूप में दीर्घकालिक भूमिका को दर्शाता था. लेकिन किसी भी अन्य गतिशील समाज की तरह, भारत की आर्थिक और जनांकिकी वास्तविकताओं में बदलाव आया है और ऐसे में सेवानिवृत्ति योजना की अवधारणा भी बदली है.
आज की बात करें तो, पेंशन की अवधारणा न केवल बदली है, बल्कि परिपक्व भी हुई है. यह सरकार समर्थित अधिकार के रूप में शुरू हुआ था, अब वह अधिक सहभागी और समावेशी ढांचे में बदल गया है, जहां व्यक्ति, संस्थान और नीतिगत परितंत्र मिलकर सेवानिवृत्ति सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करते हैं.
बड़े बदलाव
भारत की पेंशन प्रणाली दशकों तक निश्चित लाभ मॉडल पर काम करती रही, जो मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए थी. 1990 के दशक के शुरुआती आर्थिक सुधारों से एक नए युग का आरंभ हुआ. उदारीकरण ने निजी क्षेत्र के विकास को गति दी, उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया और धीरे-धीरे रोज़गार के स्वरूप को आजीवन सेवा से लचीले, गतिशील काम में बदल दिया. ऐसे में यह स्पष्ट था कि एक नए मॉडल की ज़रूरत थी, जो वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण हो, साथ ही आधुनिक कार्यबल के अनुकूल भी हो.
भारत सरकार ने 2004 में एक ऐतिहासिक सुधार किया:
नए सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत की गई. इससे एक निश्चित अंशदान मॉडल की शुरुआत हुई, जो वैश्विक रूप से प्रचलित ढांचा है. यह व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यवस्थित, दीर्घकालिक निवेश के बीच संतुलन बनाता है. इसके बाद 2009 में एनपीएस को सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया, और फिर 2015 में असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गई, जिससे देश के लाखों वंचित लोग पेंशन के दायरे में आ गए.
निष्क्रिय निर्भरता से सक्रिय भागीदारी तक
भारत में पेंशन यात्रा अब बस सीधी-सादी नीतिगत प्रक्रिया नहीं रह गई है. यह बदलते दौर की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. आज, यह सेवानिवृत्ति के बाद जीवित रहने के बारे में कम और स्वतंत्रता हासिल करने से अधिक जुड़ा है. गौरतलब है कि आज भारत में अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए सुलभ, पोर्टेबल और समावेशी पेंशन मॉडल की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है.
हाल के घटनाक्रम उत्साहजनक हैं:
- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 ने अस्थाई (गिग) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है.
- आगामी पीएफआरडीए (संशोधन) विधेयक में अधिक लचीले निवेश विकल्पों और पेंशन गारंटी कोष को मंज़ूरी मिल सकती है.
- पीएफआरडीए ने मई 2025 में, ईएनपीएस लाइट 2.0 का अनावरण किया, जो असंगठित क्षेत्र के पहली बार बचत करने वालों के लिए तैयार किया गया सरलीकृत बहुभाषी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है.
- निजी कंपनियां भी इसमें कदम रख रही हैं. अर्बन कंपनी और ज़ोमैटो जैसी कंपनियों ने गिग श्रमिकों के लिए एनपीएस खातों में स्वैच्छिक योगदान करने की शुरुआत की है.
इनमें से हर विकास न केवल नीतिगत हस्तक्षेप को दिखाता है, बल्कि बदलती जनांकिकी और काम के पैटर्न की गहरी समझ और समावेशी समाधानों के साथ पहल करने का सराहनीय प्रयास भी है.
प्रौद्योगिकी की भूमिका: विश्वास की कमी से पारदर्शी वितरण तक
भारत की पेंशन यात्रा में सबसे परिवर्तनकारी कारकों में से एक इसका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) रहा है, जो निर्बाध, पारदर्शी सेवा वितरण की रीढ़ है.
आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन ने पेंशन के लिए नाम दर्ज करना और इसमें योगदान को आसान, तेज तथा अधिक जवाबदेह बना दिया है.
आज, एक घरेलू कामगार फोन से एपीवाय के लिए पंजीकरण कर सकता है. अस्थाई कामगार (गिग वर्कर) अपने एनपीएस टियर-1 खाते में 500 रुपये का ऑटो-डेबिट कर सकता है. पेंशन, जो कभी एक अमूर्त भविष्य की अवधारणा थी, अब लोग इसे देख-परख सकते हैं, इसका हिसाब-किताब रख सकते हैं और यह वास्तविक है.
भावी योजना: पेंशन संस्कृति का अंग बने, केवल उत्पाद नहीं
फिर भी, मंजिल अभी दूर है. आज पेंशन स्वाभाविक आदत से अधिक बुनियादी ढांचे की तरह है. सबसे बड़ी बाधा सांस्कृतिक जड़ता है, यानी लोग पुरानी सोच और आदतों से बाहर नहीं निकल पाते.
हमें यह पूछना चाहिए: वर्तमान में जीने वाली पीढ़ी के लिए पेंशन को आकांक्षी कैसे बनाया जा सकता है? हम सेवानिवृत्ति योजना को केवल टिक-बॉक्स अनुपालन से दीर्घकालिक जीवन लक्ष्य में कैसे बदल सकते हैं?
इसका उत्तर है, तीन बदलाव:
- हमें पेंशन योजना को राष्ट्रीय मानस में समाहित करना होगा, जैसा हमने बैंक खातों (जन धन के जरिये) के साथ किया था.
- हमें “100-वर्षीय जीवन” के उभरते परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करना होगा – एक ऐसा भविष्य जहां लोग सेवानिवृत्ति के बाद 30 साल से अधिक समय तक, अक्सर परिवार के सहयोग के बिना, जी सकते हैं.
- और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें मजबूरी में की जाने वाली बचत के बजाय लक्ष्य-आधारित निवेश की ओर बढ़ना होगा, जहां लोग पेंशन को कटौती के रूप में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता में निवेश के रूप में देख सकें.
पेंशन फंड हाउस, नियामकों और नीति निर्माताओं की भूमिका केवल धन का प्रबंधन करना ही नहीं, बल्कि बल्कि बचतकर्ताओं में उद्देश्य, ज़िम्मेदारी और दूरदर्शिता के भाव का संचार करना भी है.
साझा भविष्य, सामूहिक लक्ष्य
भारत की पेंशन प्रणाली का विकास, प्रगति की कहानी है – एक ऐसी कहानी जहां सरकारी दूरदर्शिता, बाजार का नवोन्मेष और नागरिक सशक्तिकरण मिलकर अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करते हैं.
इसके मूल में जीवन का एक सच है कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक वित्तीय स्थिति का होना विशेषाधिकार नहीं, बल्कि यह अधिकार है. और जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करते हैं, तो हम ऐसी प्रणाली तैयार करते हैं जो न केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायसंगत हो.
आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य न केवल बेहतर उत्पादों का निर्माण करना होना चाहिए – बल्कि सुदृढ़ पेंशन संस्कृति का निर्माण करना भी होना चाहिए. ऐसी संस्कृति, जहां बचत का सम्मान हो, योजना बनाना आदत बन जाए, और सेवानिवृत्ति से डर न लगे बल्कि बस जीवन का एक चरण लगे.
किसी समाज की प्रगति का सही मापदंड केवल यह नहीं है कि वह कैसे विकसित होता है, बल्कि यह है कि वह उन लोगों की कितनी देखभाल करता है जिन्होंने इसके निर्माण में मदद की है.